Class Study : शांत क्लास में पढ़ाई हो सकती है! सीख-समझ के लिए बहस का हल्ला हो!
Nov 7, 2024, 12:37 IST
"कक्षा-कक्ष जरूरी निर्देश देने की जगह, शिक्षक निर्देशकर्ता और विद्यार्थी निष्क्रिय निर्देशग्राही। इस सम्पूर्ण व्यवस्था में शिक्षक सक्रिय रहता है लेकिन विद्यार्थी की सक्रियता नहीं होने के कारण पढ़ाई परम्परागत रूप से सुनने, पढ़ने और याद करने तक सीमित हो जाती है।" (इसी आलेख से)
RNE Special
- शांत क्लास में पढ़ाई हो सकती है! सीख-समझ के लिए बहस का हल्ला हो!
- टीचर का "बोलबाला", स्टूडेंट निष्क्रिय, सीखना और अर्थ तक पहुंचना कैसे संभव?

 ये है हमारी ढर्रे वाली क्लास : एक कमरा जिसमें विद्यार्थी बैठे हैं। एक ब्लैक बोर्ड (आजकल व्हाईट, ग्रीन या डिजीटल बोर्ड भी मिल सकते हैं) समक्ष खड़ा होकर शिक्षक पाठ पढ़ा रहा है। शिक्षक के अलावा किसी की भी आवाज नहीं आ रही। सभी विद्यार्थी ध्यानमग्न हो कर उस पाठ को सुन रहे हैं। पीरियड खत्म होने वाला है। उससे पहले टीचर कुछ होमवर्क दे रहा है। हेतु कुछ लिखित या मौखिक कार्य दिया जाएगा। अगले दिन विद्यार्थी जब आएंगे तो पहले लिखित या मौखिक कार्य नहीं करने वालों की खबर ली जाएगी। फिर आगे पहले की तरह पढ़ाई प्रारम्भ हो जाएगी। यानी सब कार्य यत्रंवत चल रहा है। कमोबेश सभी सरकारी-प्राइवेट स्कूलों में कक्षा इसी प्रकार चलती है।
ये है हमारी ढर्रे वाली क्लास : एक कमरा जिसमें विद्यार्थी बैठे हैं। एक ब्लैक बोर्ड (आजकल व्हाईट, ग्रीन या डिजीटल बोर्ड भी मिल सकते हैं) समक्ष खड़ा होकर शिक्षक पाठ पढ़ा रहा है। शिक्षक के अलावा किसी की भी आवाज नहीं आ रही। सभी विद्यार्थी ध्यानमग्न हो कर उस पाठ को सुन रहे हैं। पीरियड खत्म होने वाला है। उससे पहले टीचर कुछ होमवर्क दे रहा है। हेतु कुछ लिखित या मौखिक कार्य दिया जाएगा। अगले दिन विद्यार्थी जब आएंगे तो पहले लिखित या मौखिक कार्य नहीं करने वालों की खबर ली जाएगी। फिर आगे पहले की तरह पढ़ाई प्रारम्भ हो जाएगी। यानी सब कार्य यत्रंवत चल रहा है। कमोबेश सभी सरकारी-प्राइवेट स्कूलों में कक्षा इसी प्रकार चलती है।  बोलते शिक्षक, ताकते विद्यार्थी, सीखने को.. ??? ऐसे ही शिक्षण मॉडल के अभ्यस्त होने से हमारे लिए उपर्युक्त व्यवस्था के मायने केवल इतने बनते हैं कि कक्षा-कक्ष जरूरी निर्देश देने की जगह, शिक्षक निर्देशकर्ता और विद्यार्थी निष्क्रिय निर्देशग्राही। इस सम्पूर्ण व्यवस्था में शिक्षक सक्रिय रहता है लेकिन विद्यार्थी की सक्रियता नहीं होने के कारण पढ़ाई परम्परागत रूप से सुनने, पढ़ने और याद करने तक सीमित हो जाती है। इसमें सीखने-सिखाने के लिए बहुत अधिक गुजांईश नहीं बन पाती है।
बोलते शिक्षक, ताकते विद्यार्थी, सीखने को.. ??? ऐसे ही शिक्षण मॉडल के अभ्यस्त होने से हमारे लिए उपर्युक्त व्यवस्था के मायने केवल इतने बनते हैं कि कक्षा-कक्ष जरूरी निर्देश देने की जगह, शिक्षक निर्देशकर्ता और विद्यार्थी निष्क्रिय निर्देशग्राही। इस सम्पूर्ण व्यवस्था में शिक्षक सक्रिय रहता है लेकिन विद्यार्थी की सक्रियता नहीं होने के कारण पढ़ाई परम्परागत रूप से सुनने, पढ़ने और याद करने तक सीमित हो जाती है। इसमें सीखने-सिखाने के लिए बहुत अधिक गुजांईश नहीं बन पाती है।  रचनावादः सीखना क्या है? रचनावाद के तहत सीखना ज्ञान का निर्माण करना है। अर्थात सीखते हुए अर्थ तक पहुंचना होता है। जो कि एक सक्रिय प्रक्रिया के तहत हो सकता है। यह सक्रियता कक्षा के वातावरण से विद्यार्थी के व्यक्तिगत या सामाजिक जुड़ाव के माध्यम हो सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि कक्षा-कक्ष में शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना चाहिए। अच्छी कक्षा कौनसी? विद्यार्थी निष्क्रिय रिसेप्टर्स नहीं हैं, उसे सक्रिय रूप से सीखने में लगाए रखना चाहिए और अर्थ के निर्माण में सहायता करनी चाहिए। इसके लिए कक्षा में ऐसा वातावरण निर्माण किया जाना जरूरी है जिसमें विद्यार्थी संबंधित विषय के अर्थ और समझ का निर्माण करने के लिए संवाद में शामिल हो सकें। सन्दर्भ के आधार पर देखे तो कक्षा वही अच्छी होगी जहाँ शिक्षक व शिक्षार्थियों के बीच विषय से संबंधित संवाद चल रहा हो यानी कक्षा शांत नहीं होकर हल्के शोर-शराबे वाली होनी चाहिए। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कक्षा परम्परागत निष्क्रिय कक्षा की तरह न होकर सक्रिय कक्षा होनी चाहिए
रचनावादः सीखना क्या है? रचनावाद के तहत सीखना ज्ञान का निर्माण करना है। अर्थात सीखते हुए अर्थ तक पहुंचना होता है। जो कि एक सक्रिय प्रक्रिया के तहत हो सकता है। यह सक्रियता कक्षा के वातावरण से विद्यार्थी के व्यक्तिगत या सामाजिक जुड़ाव के माध्यम हो सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि कक्षा-कक्ष में शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना चाहिए। अच्छी कक्षा कौनसी? विद्यार्थी निष्क्रिय रिसेप्टर्स नहीं हैं, उसे सक्रिय रूप से सीखने में लगाए रखना चाहिए और अर्थ के निर्माण में सहायता करनी चाहिए। इसके लिए कक्षा में ऐसा वातावरण निर्माण किया जाना जरूरी है जिसमें विद्यार्थी संबंधित विषय के अर्थ और समझ का निर्माण करने के लिए संवाद में शामिल हो सकें। सन्दर्भ के आधार पर देखे तो कक्षा वही अच्छी होगी जहाँ शिक्षक व शिक्षार्थियों के बीच विषय से संबंधित संवाद चल रहा हो यानी कक्षा शांत नहीं होकर हल्के शोर-शराबे वाली होनी चाहिए। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कक्षा परम्परागत निष्क्रिय कक्षा की तरह न होकर सक्रिय कक्षा होनी चाहिए  सफल विद्यालय की नींव है सकारात्मकता की संस्कृतिः एक स्वस्थ, सफल विद्यालय की नींव में सकारात्मकता की उर्जा होती है। यह सकारात्मकता स्कूल के भीतर शिक्षकों से लेकर विद्यार्थियों तक, विद्यालय के अन्य कर्मियों व यहाँ तक कि विद्यालय में आने वाले अभिभावकों तक में दिखाई देनी चाहिए है। क्या है सकारात्मकता की संस्कृति? : सामान्य तौर पर सकारात्मकता को सरलता, दूसरों के विचारों को सुनना और विपरीत समय में शांत रहकर कार्य करने के सन्दर्भों में ही लिया जाता है। लेकिन सकारात्मकता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू खुशी और उत्साह है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सकारात्मकता आशावाद की नींव है। सकारात्मक दृष्टिकोण जो अल्प तनाव के साथ लचीलापन लिए हुए समस्या-समाधान बेहतर कौशल और उपलब्धि के उच्च स्तर के रूप में प्रकट हो सकती है। इसमें कोई दोराय नहीं हो सकती कि एक सकारात्मक आशावादी व्यक्ति जीवन दोनों में चुनौतियों से निपटने के लिए स्वतः ही प्रेरित होता है।
सफल विद्यालय की नींव है सकारात्मकता की संस्कृतिः एक स्वस्थ, सफल विद्यालय की नींव में सकारात्मकता की उर्जा होती है। यह सकारात्मकता स्कूल के भीतर शिक्षकों से लेकर विद्यार्थियों तक, विद्यालय के अन्य कर्मियों व यहाँ तक कि विद्यालय में आने वाले अभिभावकों तक में दिखाई देनी चाहिए है। क्या है सकारात्मकता की संस्कृति? : सामान्य तौर पर सकारात्मकता को सरलता, दूसरों के विचारों को सुनना और विपरीत समय में शांत रहकर कार्य करने के सन्दर्भों में ही लिया जाता है। लेकिन सकारात्मकता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू खुशी और उत्साह है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सकारात्मकता आशावाद की नींव है। सकारात्मक दृष्टिकोण जो अल्प तनाव के साथ लचीलापन लिए हुए समस्या-समाधान बेहतर कौशल और उपलब्धि के उच्च स्तर के रूप में प्रकट हो सकती है। इसमें कोई दोराय नहीं हो सकती कि एक सकारात्मक आशावादी व्यक्ति जीवन दोनों में चुनौतियों से निपटने के लिए स्वतः ही प्रेरित होता है। 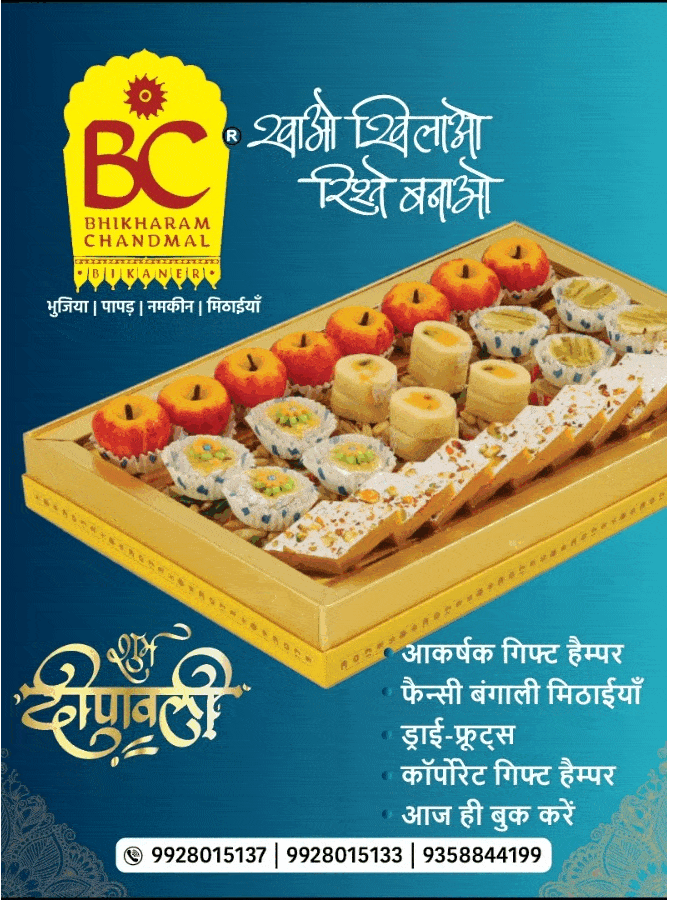 कैसे होगा सकारात्मक संस्कृति का निर्माण?ः शिक्षा के सन्दर्भ में बात करें तो विद्यालय और कक्षा में सकारात्मक वातावरण का विकास शिक्षकों और विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण समय में प्रगति करने में सक्षम बनाता है। विद्यालय में सकारात्मक संस्कृति का निर्माण कक्षा-कक्ष से प्रारम्भ होता है और फिर ये पूरे विद्यालय में फैलता है। इसके लिए जरूरी है कि संस्था प्रधान कुशल नेतृत्वकर्ता हो। वह लगातार अपने साथी शिक्षकों से शैक्षणिक मुददों व अन्य विद्यालयी मुद्दों पर नियमित चर्चा हो। संस्था प्रधान समाज के साथ भी नियमित चर्चा के प्रस्तुत होना चाहिए। समय-समय पर एसडीएमसी, एसएमसी और पीटीम के माध्यम से नियमित संवाद बनाकर विद्यालय के शैक्षणिक और भौतिक उत्थान हेतु प्रयासरत रहना चाहिए। इसके अलावा षिक्षकों को कक्षा में संवाद यानी शिक्षकों और विद्यार्थियों व विद्यार्थियों और विद्यार्थियों के मध्य संवाद को प्रेरित करना चाहिए। कक्षा में सभी बच्चे खुलकर अपनी बात रख सकें ऐसा माहौल बनाया जाने हेतु शिक्षक को प्रयास करने चाहिए। जीवंत कक्षा कैसी हो? : कक्षा में बैठकर व्याख्यान सुनते हुए विद्यार्थी का मन को भटक सकता है। यदि वह सामान्य श्रोता बना रहता है तो वह बोरियत महसुस करते हुए झपकी ले सकता है। ऐसा हमारे साथ भी होता है। इसलिए जरूरी है कि कक्षा को जीवंत बनाया जाए। जीवंत कक्षा में विद्यार्थी को निष्क्रिय श्रोता के स्थान पर सक्रिय रिसेप्टर में बदलना जरूरी है। इसके लिए सबसे जरूरी बात कक्षा में संवाद होना चाहिए।
कैसे होगा सकारात्मक संस्कृति का निर्माण?ः शिक्षा के सन्दर्भ में बात करें तो विद्यालय और कक्षा में सकारात्मक वातावरण का विकास शिक्षकों और विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण समय में प्रगति करने में सक्षम बनाता है। विद्यालय में सकारात्मक संस्कृति का निर्माण कक्षा-कक्ष से प्रारम्भ होता है और फिर ये पूरे विद्यालय में फैलता है। इसके लिए जरूरी है कि संस्था प्रधान कुशल नेतृत्वकर्ता हो। वह लगातार अपने साथी शिक्षकों से शैक्षणिक मुददों व अन्य विद्यालयी मुद्दों पर नियमित चर्चा हो। संस्था प्रधान समाज के साथ भी नियमित चर्चा के प्रस्तुत होना चाहिए। समय-समय पर एसडीएमसी, एसएमसी और पीटीम के माध्यम से नियमित संवाद बनाकर विद्यालय के शैक्षणिक और भौतिक उत्थान हेतु प्रयासरत रहना चाहिए। इसके अलावा षिक्षकों को कक्षा में संवाद यानी शिक्षकों और विद्यार्थियों व विद्यार्थियों और विद्यार्थियों के मध्य संवाद को प्रेरित करना चाहिए। कक्षा में सभी बच्चे खुलकर अपनी बात रख सकें ऐसा माहौल बनाया जाने हेतु शिक्षक को प्रयास करने चाहिए। जीवंत कक्षा कैसी हो? : कक्षा में बैठकर व्याख्यान सुनते हुए विद्यार्थी का मन को भटक सकता है। यदि वह सामान्य श्रोता बना रहता है तो वह बोरियत महसुस करते हुए झपकी ले सकता है। ऐसा हमारे साथ भी होता है। इसलिए जरूरी है कि कक्षा को जीवंत बनाया जाए। जीवंत कक्षा में विद्यार्थी को निष्क्रिय श्रोता के स्थान पर सक्रिय रिसेप्टर में बदलना जरूरी है। इसके लिए सबसे जरूरी बात कक्षा में संवाद होना चाहिए।  क्यों जरूरी है कक्षा में संवाद?ः सीखने की प्रक्रिया गलतियों और बाधाओं से भरी होती है। इसलिए कक्षा-कक्षा में विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच बातचीत और चर्चा होना आवष्यक है। यदि संवाद होगा तो विद्यार्थी को लगातार संबंलन प्राप्त होता रहेगा जिससे सीखने में आने असफलता, सफलता पर हावी नहीं होगी। कक्षा में संवाद से क्या लाभ हो सकते हैंः सामान्यतः हम समझते है कि विद्यार्थी कक्षा-कक्ष में शिक्षण के दौरान अपनी समझ बना रहे होते हैं। लेकिन यह अर्द्धसत्य है। बहुत से विद्यार्थी किसी अवधारणा के प्रति समझ बनाने में परेशानी महसुस कर रहे होते। इस परेशानी को समझने के लिए कक्षा में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए सार्थक संवाद से निम्नांकित लाभ हो सकते हैं।
क्यों जरूरी है कक्षा में संवाद?ः सीखने की प्रक्रिया गलतियों और बाधाओं से भरी होती है। इसलिए कक्षा-कक्षा में विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच बातचीत और चर्चा होना आवष्यक है। यदि संवाद होगा तो विद्यार्थी को लगातार संबंलन प्राप्त होता रहेगा जिससे सीखने में आने असफलता, सफलता पर हावी नहीं होगी। कक्षा में संवाद से क्या लाभ हो सकते हैंः सामान्यतः हम समझते है कि विद्यार्थी कक्षा-कक्ष में शिक्षण के दौरान अपनी समझ बना रहे होते हैं। लेकिन यह अर्द्धसत्य है। बहुत से विद्यार्थी किसी अवधारणा के प्रति समझ बनाने में परेशानी महसुस कर रहे होते। इस परेशानी को समझने के लिए कक्षा में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए सार्थक संवाद से निम्नांकित लाभ हो सकते हैं।  1. कमियों को समझकर सीखने को मजबूत बनानाः कक्षा में संवाद छात्रों को अपनी समझ को शब्दों में व्यक्त करने, अपने विचारों को सामने लाने और उन्हें बारीकी से परखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। संवाद में शामिल होकर छात्र ज्ञान के कमियों की पहचान कर सकते हैं। अपनी धारणाओं को चुनौती दे सकते हैं। इस प्रकार कमियों के उजागर होने से शिक्षक और अपने साथियों की मदद से अपनी समझ को मजबूत कर सकते हैं। 2. याद करने की क्षमता में सुधारः यह सही है कि शिक्षा का मतलब रटना नहीं है। लेकिन कुछ सन्दर्भों पर अपनी स्मृति को मजबूत बनाए बगैर सीखना मजबूत नहीं हो सकता है। आज की तेज गति के दूरसंचार और आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस की सुविधा मोबाइल के माध्यम से हाथों में उपलब्ध होने के कारण आज विद्यार्थी कि प्रत्येक अवधारणा के लिए प्रोद्योगिकी पर निर्भरता बढ़ने के कारण स्मृति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कक्षा में संवाद इस प्रकार दुष्प्रभावों को कम कर सकता है। जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से बातचीत में भाग लेते हैं और मौखिक रूप से जानकारी संसाधित करते हैं, तो वे तंत्रिका आवेग मजबूत होते हैं। जिसके परिणामस्वरूप संवाद समाप्ति के पश्चात भी जानकारी उनके साथ बनी रहेगी। इससे उनकी याद करने की क्षमता में वृद्धि होगी। 3. सीखने में संलग्नता बढ़नाः कक्षा में बातचीत और चर्चा के चलते विद्यार्थी सूचना के निष्क्रिय रिसेप्टर से कहीं अधिक सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। कक्षा में बातचीत विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, अपने दृष्टिकोण साझा करने और सामूहिक चर्चा में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब विद्यार्थी स्वयं बोल रहा हो और कक्षा में बातचीत के दौरान सक्रियता से सुन रहा हो तो सीखने में संलग्नता के चलता उसका ध्यान विषय पर केन्द्रित रहता है। जिसके परिणामस्वरूप सीखना मजबूत होता है।
1. कमियों को समझकर सीखने को मजबूत बनानाः कक्षा में संवाद छात्रों को अपनी समझ को शब्दों में व्यक्त करने, अपने विचारों को सामने लाने और उन्हें बारीकी से परखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। संवाद में शामिल होकर छात्र ज्ञान के कमियों की पहचान कर सकते हैं। अपनी धारणाओं को चुनौती दे सकते हैं। इस प्रकार कमियों के उजागर होने से शिक्षक और अपने साथियों की मदद से अपनी समझ को मजबूत कर सकते हैं। 2. याद करने की क्षमता में सुधारः यह सही है कि शिक्षा का मतलब रटना नहीं है। लेकिन कुछ सन्दर्भों पर अपनी स्मृति को मजबूत बनाए बगैर सीखना मजबूत नहीं हो सकता है। आज की तेज गति के दूरसंचार और आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस की सुविधा मोबाइल के माध्यम से हाथों में उपलब्ध होने के कारण आज विद्यार्थी कि प्रत्येक अवधारणा के लिए प्रोद्योगिकी पर निर्भरता बढ़ने के कारण स्मृति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कक्षा में संवाद इस प्रकार दुष्प्रभावों को कम कर सकता है। जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से बातचीत में भाग लेते हैं और मौखिक रूप से जानकारी संसाधित करते हैं, तो वे तंत्रिका आवेग मजबूत होते हैं। जिसके परिणामस्वरूप संवाद समाप्ति के पश्चात भी जानकारी उनके साथ बनी रहेगी। इससे उनकी याद करने की क्षमता में वृद्धि होगी। 3. सीखने में संलग्नता बढ़नाः कक्षा में बातचीत और चर्चा के चलते विद्यार्थी सूचना के निष्क्रिय रिसेप्टर से कहीं अधिक सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। कक्षा में बातचीत विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, अपने दृष्टिकोण साझा करने और सामूहिक चर्चा में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब विद्यार्थी स्वयं बोल रहा हो और कक्षा में बातचीत के दौरान सक्रियता से सुन रहा हो तो सीखने में संलग्नता के चलता उसका ध्यान विषय पर केन्द्रित रहता है। जिसके परिणामस्वरूप सीखना मजबूत होता है। डा.प्रमोद चमोली के बारे में:



